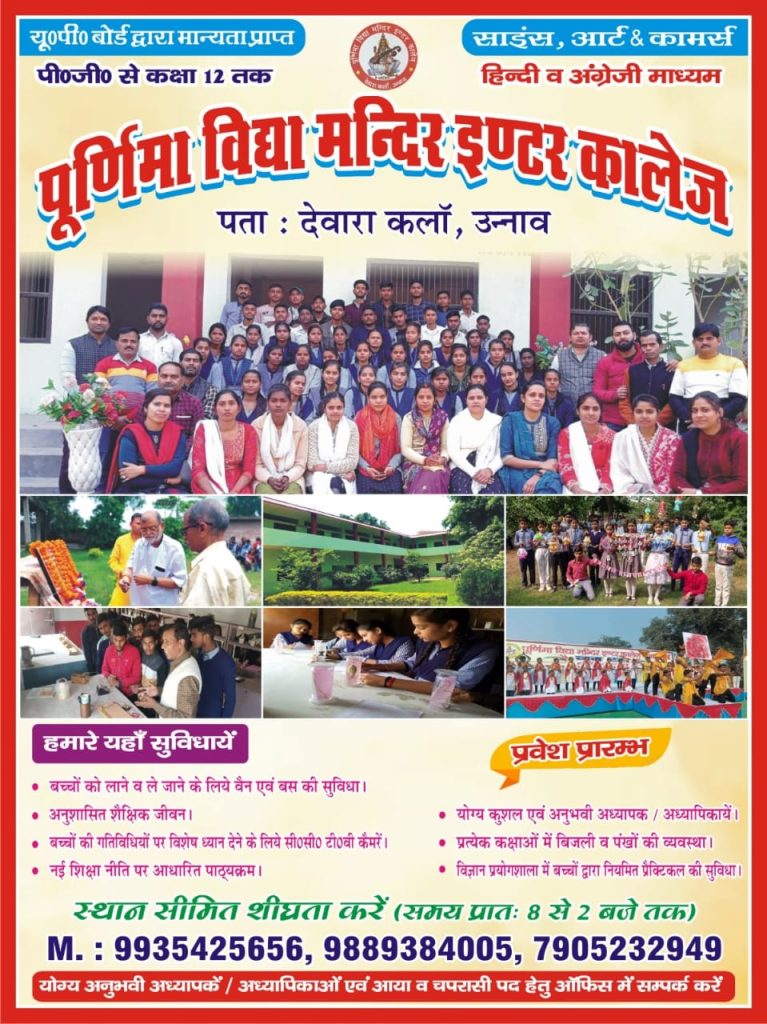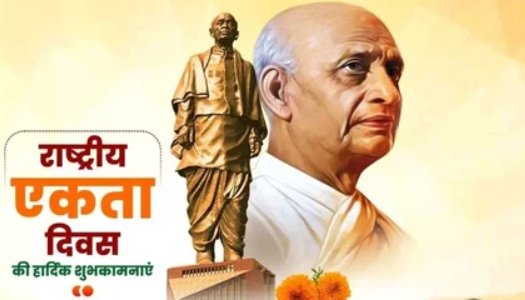अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच अचानक भड़की सीमा झड़पों ने एक बार फिर पूरे एशिया को अस्थिरता के डर में डाल दिया है। दोनों देशों के बीच तकरार नई नहीं है, पर इस बार हालात ऐसे मोड़ पर पहुँच गए हैं जहाँ हर गोलाबारी सिर्फ़ सैनिकों की नहीं, बल्कि सीमाओं पर रहने वाले आम नागरिकों की ज़िंदगियों पर भी चोट कर रही है। सवाल यह है कि क्या दक्षिण एशिया एक और युद्ध की तरफ़ बढ़ रहा है — या अब भी कोई राह बची है शांति की?
संघर्ष की शुरुआत:
पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफ़ग़ान क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए सीमापार हवाई कार्रवाई की। जवाब में काबुल प्रशासन ने कहा कि पाकिस्तान ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है और अफ़ग़ान चौकियों पर हमले हुए हैं। नतीजा — सीमा के टोरख़म और चमन इलाकों में ज़बरदस्त गोलाबारी, बंद व्यापार मार्ग, और सैकड़ों लोगों का विस्थापन।
यह तनाव दरअसल उस पुराने घाव से रिस रहा है, जिसे कभी भरा ही नहीं गया — यानी Durand Line का विवाद। यह रेखा, जो 1893 में ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई थी, आज भी दोनों मुल्कों के बीच अविश्वास की दीवार बनी हुई है।
इतिहास की परतें:
सोवियत आक्रमण (1979), अमेरिका का प्रवेश (2001), और 2021 में विदेशी सेनाओं की वापसी — इन तीनों घटनाओं ने अफ़ग़ानिस्तान को बार-बार अशांत किया। हर बार पाकिस्तान को सुरक्षा और शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद उम्मीद थी कि दोनों इस्लामी पड़ोसी रिश्तों को नया रूप देंगे, लेकिन हकीकत यह रही कि Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) जैसे चरमपंथी समूहों को लेकर दोनों के बीच संदेह और गहराता गया। पाकिस्तान का आरोप है कि अफ़ग़ान ज़मीन से TTP को संरक्षण मिल रहा है; अफ़ग़ान तालिबान इन आरोपों से इनकार करते हैं।
आज की स्थिति:
दोनों देशों की सीमाओं पर गोलीबारी के साथ-साथ एक “सूक्ष्म युद्ध” चल रहा है — सोशल मीडिया पर बयानबाज़ी, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आरोप-प्रत्यारोप, और आर्थिक दबाव की रणनीतियाँ। पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता और अफ़ग़ानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय मान्यता की कमी इस संघर्ष को और पेचीदा बना रही है।
क्षेत्रीय विश्लेषक मानते हैं कि यदि यह टकराव लंबा खिंचा तो परिणाम सिर्फ़ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य एशिया से लेकर खाड़ी देशों तक व्यापारिक मार्ग बाधित होंगे, शरणार्थियों की नई लहर उठेगी, और पहले से तनावग्रस्त दक्षिण एशिया की सामरिक शांति बुरी तरह प्रभावित होगी।
सेंसरशिप की प्रासंगिकता और विरोधाभास: एक वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य
आगे की दिशा:
- कूटनीतिक हस्तक्षेप: क़तर, सऊदी अरब, चीन और रूस जैसे देशों की मध्यस्थ भूमिका अहम हो सकती है। पहले भी ऐसे संघर्ष इन्हीं देशों के प्रयासों से थमे हैं।
- सीमावर्ती विकास और विश्वास-निर्माण: युद्धविराम के बाद दोनों देशों को सीमा-पार व्यापार और स्थानीय जनजातीय भागीदारी को बढ़ाना होगा। यही दीर्घकालिक शांति का व्यावहारिक रास्ता है।
- TTP जैसे समूहों पर साझा रणनीति: गैर-राज्य आतंकी संगठनों पर संयुक्त कार्रवाई के बिना शांति असंभव है।
- मानवीय गलियारे खोलना: आम नागरिकों की सुरक्षा और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मानवीय मार्ग स्थापित करना तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए।
राम मनोहर लोहिया: सामाजिक चेतना का शिल्पकार
एशिया के लिए शांति का संदेश:
पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान का यह संघर्ष दो राष्ट्रों का नहीं, बल्कि एक साझा इतिहास का अंतहीन बोझ है। सीमाओं के दोनों ओर रहने वाले लोग एक ही दर्द, एक ही भाषा और एक ही उम्मीद साझा करते हैं — अमन की।
इसलिए यह क्षण युद्ध की भाषा नहीं, वार्ता की ज़रूरत का है। अब वक्त है कि दोनों सरकारें हथियारों से नहीं, संवाद से जवाब दें। एशिया की स्थिरता और मानवता की सुरक्षा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है।
अब एक ही अपील — युद्धविराम हो। सीमा पर फिर से इंसानियत का परचम लहराए, ताकि यह धरती बारूद नहीं, भरोसे की खुशबू से महके।
कुछ पुस्तक जो आप पढ़ सकते है दोनों देशों की जानकारी के लिए –
- “Pakistan: Courting the Abyss” – Tilak Devasher (Right-wing / security perspective)
- “Afghanistan and Pakistan: Conflict, Extremism and Resistance to Modernity” – Riaz Mohammad Khan (Conservative diplomatic view)
- “Ghost Wars” – Steve Coll (Liberal/Left investigative perspective)
- “The Great Game: The Struggle for Empire in Central Asia” – Peter Hopkirk (Historical-geopolitical classic, neutral to right-leaning)
- “Descent into Chaos” – Ahmed Rashid (Left-liberal, critical of U.S.–Pakistan–Taliban nexus)