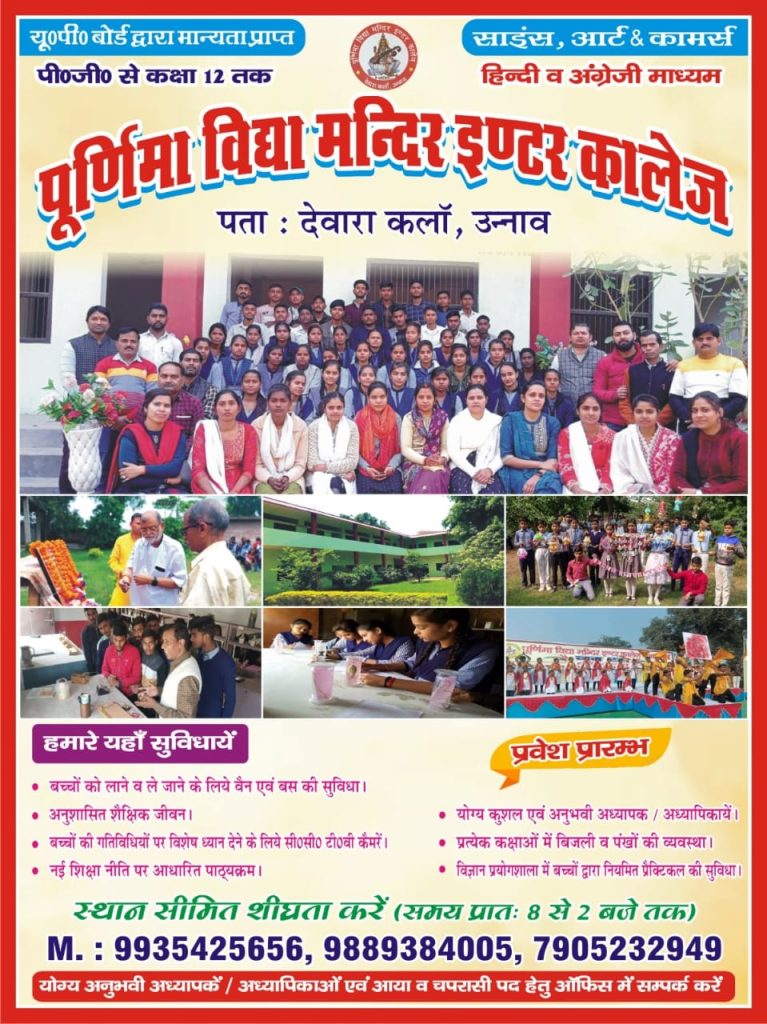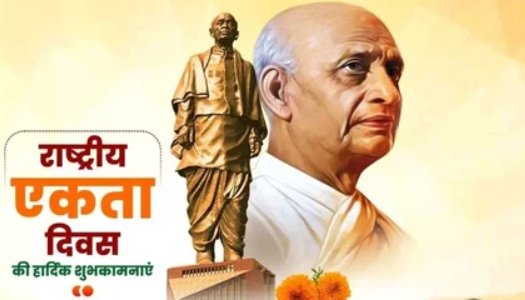चेतावनी जो केवल मौसम नहीं, व्यवस्था से भी जुड़ी है
बंगाल की खाड़ी पर उठता मोंथा तूफ़ान इस बार केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं — यह हमारे समय का पर्यावरणीय इशारा है।
हवा की रफ्तार जब 100 किमी प्रतिघंटा पार करती है, तो यह सिर्फ़ पेड़ नहीं गिराती — यह हमें बताती है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का ख़तरा नहीं, वर्तमान का संकट है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मोंथा को “गंभीर चक्रवाती तूफ़ान” की श्रेणी में रखा है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय ज़िलों में प्रशासन ने अब तक 50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।
समुद्र का स्तर बढ़ा है, और लहरें उन तटों को काट रही हैं जहाँ कभी बच्चे क्रिकेट खेला करते थे।
मोंथा: एक तूफ़ान नहीं, बल्कि पैटर्न का हिस्सा
2024 में भारत के तटीय इलाकों ने 12 से ज़्यादा गंभीर चक्रवातीय घटनाएँ झेली हैं — जिनमें से ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी से निकलीं।
IMD और IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) के वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र की सतह का तापमान अब औसतन 0.2°C प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है।
यही कारण है कि तूफ़ानों की संख्या नहीं, उनकी तीव्रता और जीवनकाल बढ़ रहे हैं।
पहले जहां तूफ़ान 12 घंटे में शांत हो जाते थे, अब वे 36 घंटे तक सक्रिय रहते हैं।
मानवीय संकट: ‘क्लाइमेट रिफ्यूजी’ का नया भारत
मोंथा जैसे तूफ़ान केवल तट नहीं उजाड़ते — ये लोगों की पहचान छीन लेते हैं।
भारत में हर साल लगभग 50 लाख लोग बाढ़, चक्रवात और तटीय कटाव के कारण विस्थापित होते हैं।
UNHCR की रिपोर्ट बताती है कि यह संख्या अगले दशक में 1.5 करोड़ तक पहुँच सकती है।
इनमें अधिकांश गरीब और मछुआरा समुदाय से आते हैं — जो अपने गांव छोड़कर शहरों में आकर “क्लाइमेट रिफ्यूजी” कहलाने लगते हैं।
यह शब्द अभी हमारी नीतियों में शामिल नहीं है, लेकिन हकीकत में ये भारत के सबसे बड़े विस्थापित समूहों में से एक हैं।
क्यों बढ़ रही हैं ऐसी आपदाएँ?
- समुद्री तापमान में वृद्धि: समुद्र जितना गर्म होगा, तूफ़ान उतना अधिक ऊर्जा सोखेगा।
- मॉनसून की अनिश्चितता: दक्षिण-पूर्वी हवाओं में बदलाव ने बंगाल की खाड़ी को “साइक्लोन लैब” बना दिया है।
- मैनग्रोव और वनस्पति का नाश: ये प्राकृतिक दीवारें खत्म हो चुकी हैं, जिससे लहरें सीधे बस्तियों से टकराती हैं।
- शहरीकरण और कंक्रीट कोस्टलाइन: तटीय शहरों में जलनिकासी और हरित आवरण का ह्रास।
दुनिया की स्थिति: बढ़ता मौसमीय असंतुलन
- अमेरिका में हरिकेन हेलीन ने लाखों लोगों को बेघर किया।
- जापान और फिलीपींस हर साल औसतन 8-10 टायफून झेलते हैं।
- अफ्रीका में “Idai” और “Freddy” जैसे तूफ़ान ने भोजन और जल संकट को चरम पर पहुंचाया।
UN के अनुमान के मुताबिक़ 2050 तक 21.6 करोड़ लोग जलवायु कारणों से अपना घर छोड़ने को मजबूर होंगे।
इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र — एशिया-प्रशांत — यानी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया होंगे।
SIR का इतिहास: मतदाता-सूची की सफाई
भारत को क्या करना चाहिए: पाँच-स्तरीय रोडमैप
1️⃣ तटीय सुरक्षा का पुनर्निर्माण
मैनग्रोव और समुद्री पौधों की पुनर्स्थापना, तटीय बफर ज़ोन और समुद्री दीवारों की स्मार्ट निगरानी।
2️⃣ ‘क्लाइमेट रिफ्यूजी’ नीति बनाना
विस्थापितों के लिए रोजगार, शिक्षा और पुनर्वास का अधिकार सुनिश्चित करना।
आज वे “आपदा पीड़ित” कहलाते हैं, पर कल उन्हें “जलवायु नागरिक” का दर्जा देना होगा।
3️⃣ टेक्नोलॉजी आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम
ड्रोन और सैटेलाइट डेटा के साथ ‘मोबाइल सायरन नेटवर्क’ — ताकि हर मछुआरे और गांव तक अलर्ट पहुंच सके।
4️⃣ स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना
आपदा से पहले प्रशिक्षण, राहत वितरण में स्थानीय भागीदारी और महिला स्वयंसेवक नेटवर्क।
5️⃣ नीति स्तर पर जलवायु-न्याय (Climate Justice)
बड़ी कंपनियों से ‘कार्बन टैक्स’ लेकर उन समुदायों में निवेश करना जो हर साल प्राकृतिक आपदाएँ झेलते हैं।
कानूनों की नई परिभाषा: BJP-NDA सरकार का “नए भारत” का विधायी रोडमैप
तूफ़ान चेतावनी है, समाधान की पुकार भी
Cyclone मोंथा हमें केवल डराता नहीं — यह याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता एकतरफा नहीं हो सकता।
विकास का अर्थ यह नहीं कि हम समुद्र को चुनौती दें, बल्कि यह समझें कि समुद्र भी हमें सीमाएँ दिखा रहा है।
सवाल यह नहीं कि अगला तूफ़ान कब आएगा — सवाल यह है कि जब आएगा, क्या हम तैयार होंगे या फिर वही गलती दोहराएँगे?
लेखक की टिप्पणी
भारत के सामने अब दो रास्ते हैं — या तो जलवायु संकट को नीति के केंद्र में लाए, या हर साल नई आपदाओं के बाद पुराने वादों को दोहराए।
‘मोंथा’ हमें रोकने नहीं, सोचने आया है।